TNF News
बिहार में जल संकट: 1950 के दशक से लेकर आज तक।

बिहार: बिहार में आजादी के बाद 1950-51-52 में भयंकर अकाल जैसी स्थिति बन गई थी। अकाल घोषित तो नहीं हुआ था, पर परिस्थितियां कम भयावह भी नहीं थीं। तब म्यांमार जैसे छोटे-छोटे मुल्कों से भी अनाज मंगवाना पड़ा था। उस अकाल की गाथा खोजते-खोजते हमारी भेंट रोहतास जिले के लहेरी गांव, प्रखंड सासाराम के एक 88 वर्षीय बुजुर्ग शिवपूजन सिंह से हुई। उन्होंने लंबी वार्ता के दौरान बताया कि तब तो हम लोग बच्चे ही थे, फिर भी बहुत सी बातें याद हैं। ‘हमारे पीने के पानी की कमी उस सूखे के समय भी नहीं हुई थी। पानी कुएं में हमेशा मिल जाता था, क्योंकि तालाब भले ही सूख जाएं, कुआं कभी नहीं सूखता था। जानवरों को भी वही पानी दिया जाता था। अब तो कुएं बचे ही नहीं हैं और उनके नष्ट हो जाने की एक वजह है कि उन दिनों आज की तरह बोरिंग नहीं थी।’
इस घटना के 70-75 साल बाद अब जो नदियों, तालाबों, झरनों और अन्य जल-स्रोतों की जो दुर्दशा हुई है, वह चिंताजनक है। केंद्रीय जल आयोग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 150 प्रमुख जलाशयों का जलस्तर 23 फीसदी कम हो गया है और यहां पिछले साल की तुलना में 77 फीसदी ही पानी है। इतना ही नहीं, इनमें से चार जलाशय मार्च में सूख गए थे। यह गंभीर होते जल संकट का स्पष्ट संकेत है। अब पानी के लिए इस कदर मारामारी है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की खबरें रोजाना अखबारों में छप रही हैं। बेशक, इसके कारण अलग-अलग हो सकते हैं। कुओं की जगह ले चुके बोरिंग, लिफ्ट आदि आधुनिक संयंत्रों ने पानी की उपलब्धता उन लोगों के लिए बढ़ाई है, जो इसकी कीमत अदा कर सकते हैं। आज से लगभग बीस साल पहले गुजरात से यह पहली सूचना मिलने लगी थी कि अगर किसी गरीब आदमी के बगल में बड़े आदमी के खेत हों, तो छोटे किसान की बोरिंग सूख जाती थी, क्योंकि वह समृद्ध किसान की बोरिंग के मुकाबले और गहरे स्तर तक जाने की कीमत नहीं चुका सकता था।
नदियों के उद्गम के आसपास बने जलाशयों ने पानी के वितरण और निचले क्षेत्रों में उसकी उपलब्धता पर प्रश्न-चिह्न लगाए हैं। 1960 के उत्तराद्र्ध से आधुनिक खेती के विस्तार से सिंचाई के उपयोग में आने वाले पानी की मांग बेतहाशा बढ़ गई है। इस पानी के उपयोग से जहां एक ओर कृषि उत्पादन बढ़ा, तो दूसरी ओर बहुत सी खेती की जमीन पर लवणीयता भी बढ़ी है, जिससे उन क्षेत्रों में उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। पिछले कृषि वर्ष में हरियाणा और दिल्ली के बीच यमुना के पानी को लेकर बाढ़ और सूखे, दोनों मौसम में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले तंत्र की भूमिका आलोचना के दायरे में रही। अभी ही दिल्ली में जो जल संकट है, वह जल-तंत्र की विफलता की ओर इशारा करता है और बताता है कि जरूरतमंदों तक पानी पहुंचाने की हमारी कवायद किस कदर ध्वस्त हो चुकी है। जब नदी से पीने के लिए पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही, तो इस विफलता की जिम्मेदारी क्या तय नहीं होनी चाहिए?
यह भी पढ़े :विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर नवयुगदल को सम्मानित किया गया।
सवाल विभाग की प्राथमिकताओं का भी है। शताब्दी के प्रारंभ में पटना में गंगा के किनारे एक मैरीन ड्राइव बनाने की योजना किसी को भी आकर्षक लगती थी। मगर यह भी सच था कि राज्य की शिक्षित जनता का आंकड़ा कमोबेश वही था, जो देश के स्तर पर 1961 में था। मैरिन ड्राइव के प्रस्ताव पर आह्लादित होने वाली जनता में से शायद ही किसी ने यह आवाज उठाई कि मैरिन ड्राइव बनाने से पहले शिक्षा के सुधार का कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिए था। यह मैरिन ड्राइव अब बन चुका है और सफल भी है, लेकिन प्राथमिकता की बात करें, तो पहले कुछ और होना चाहिए था।
बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं का अलग ही किस्सा है। विभाग आजादी के बाद से नदियों के किनारे तटबंध बनाने के अलावा कुछ कर नहीं पाया है, जबकि देश का बाढ़ प्रवण क्षेत्र, यानी किसी न किसी समय बाढ़ से प्रभावित होने वाला इलाका, आजादी के बाद से 12वीं योजना बीत जाने के बाद दोगुना हो गया है। बिहार का 68.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण है, जो आजादी के समय केवल 25 लाख हेक्टेयर था। राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 50 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण है, जो आजादी के समय इसका आधा था। अब तो शहरों की बाढ़ नई समस्या का रूप ले चुकी है।
जल-संकट का प्रशासनिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कोई सिंचाई या बाढ़ नियंत्रण की योजना तैयार की जाती है, तो उसके कुछ उद्देश्य, पूरा होने का समय, लागत खर्च आदि की व्याख्या की जाती है और उसके बाद लाभ-लागत गुणक निर्धारित किया जाता है कि योजना पर जो खर्च किया जाएगा, उसके अनुरूप लाभ कितना होगा? इतनी सूचना राज्यों की विधानसभा में राज्यपाल के बजट भाषण में जरूर बताई जाती है। इस पर बहस भी होती है और अगर उसमें कोई सुधार या परिवर्तन की आवाज उठती है, तो उसका संज्ञान लिया जाता है। बताते हैं कि विधानसभा में जब बजट और कार्यक्रम पर बहस होती है, तब वहां से जो भी प्रश्न उठते हैं, उनको मुख्य अभियंताओं को भेज दिया जाता है, जिस पर वे अपना मंतव्य देकर वापस कर देते हैं।
यह भी पढ़े :गांधी वाटिका एवं म्यूजियम सेंट्रल पार्क खुलवाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन
आश्चर्यजनक रूप से बजट प्रस्ताव और उस पर हुई बहस को लेकर इन अधिकारियों की कोई अलग से बैठक नहीं होती और ज्यादातर काम विभागीय स्तर पर कर लिया जाता है।
स्पष्ट है, हमारी मूल समस्या जवाबदेही की है कि व्यवस्था जो कुछ भी हासिल करने का विचार रखती है, उन उद्देश्यों की पूर्ति हो पाती है या नहीं? इसके लिए अंगरेजी में ‘अकाउंट’ और ‘अकाउंटेबिलिटी’ जैसे शब्दों का उपयोग होता है। ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर हैं नहीं। अकाउंट लेखा-जोखा है, जबकि अकाउंटेबिलिटी जिम्मेवारी है। ऑडिट के बाद अकाउंट का काम प्राय: समाप्त हो जाता है, पर अकाउंटेबिलिटी तब तक पीछा नहीं छोड़ती, जब तक उद्देश्य पूरे न हो जाएं। जल संकट का यही निदान है। संबंधित विभागों को सोचना चाहिए कि क्या 1950 के दशक की परिस्थितियों से निपट लेने के हम सक्षम हो पाए हैं?
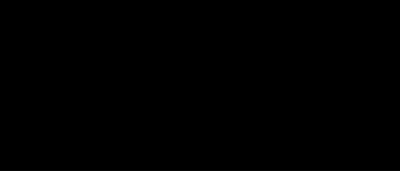
 Big Breaking: डैम में तैरता मिला अज्ञात युवती का शव, इलाके में सनसनी
Big Breaking: डैम में तैरता मिला अज्ञात युवती का शव, इलाके में सनसनी
 केरल तट पर डूबा लाइबेरियाई जहाज, तेल रिसाव का बड़ा खतरा | तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी
केरल तट पर डूबा लाइबेरियाई जहाज, तेल रिसाव का बड़ा खतरा | तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी Rashtriya Patrkar Media Sangathan (RPMS): राष्ट्रीय पत्रकार मीडिया संगठन की पहली औपचारिक बैठक का सफल आयोजन
Rashtriya Patrkar Media Sangathan (RPMS): राष्ट्रीय पत्रकार मीडिया संगठन की पहली औपचारिक बैठक का सफल आयोजन